बातें ::
दलपत सिंह राजपुरोहित
से
जे सुशील
दलपत सिंह राजपुरोहित यूनिवर्सिटी ऑफ़ टेक्सास (ऑस्टिन) में असिस्टेंट प्रोफ़ेसर हैं। दलपत अपनी यूनिवर्सिटी में हिंदी साहित्य, दक्षिण एशिया का इतिहास, भाषा और संस्कृति से जुड़े विषय पढ़ाते हैं। इससे पहले वह प्रतिष्ठित कोलंबिया विश्वविद्यालय में लंबे समय तक हिंदी और उर्दू पढ़ा चुके हैं। हाल ही में प्रकाशित उनकी पुस्तक ‘सुंदर के स्वप्न’ (राजकमल प्रकाशन, 2022) ख़ासी चर्चित रही है। इसके बाद उनकी पुस्तक ‘इन द श्राइन ऑफ़ द हार्ट : सन्त्स ऑफ़ राजस्थान’ भी आई है, जिसे उन्होंने मोनिका हॉर्स्ट्मैन के साथ लिखा है। दलपत की रुचि हिंदी भाषा और साहित्य के शुरुआती इतिहास, भक्ति कविता, मठों और दरबारों में रचे जाने वाले साहित्य में रही है। यहाँ प्रस्तुत बातचीत इन्हीं विषयों पर, ख़ासकर उनकी किताब ‘सुंदर के स्वप्न’ पर एकाग्र है। यह बातचीत प्रथमतः ऑडियो-वीडियो फ़ॉर्म में ‘अंजुमन तरक़्क़ी-उर्दू (हिंद)’ के लिए की गई थी।
— जे सुशील

जे
दलपत पहले तो यह बताएँ कि आप भारत में कहाँ से हैं और भारत से अमेरिका में प्रोफ़ेसर बनने का सफ़र कैसे तय किया आपने?
दलपत
मैं राजस्थान के पाली ज़िले के एक छोटे से गाँव सोकड़ा से हूँ। स्कूली शिक्षा वहीं हुई। फिर फ़ालना में और वहाँ से जोधपुर आया, जहाँ मेरे बड़े भाई प्रेम सिंह भी पढ़ते थे। बड़े भाई के साथ बिहार के कुछ छात्र थे, जिनसे जेएनयू के बारे में पता चला। जेएनयू का परीक्षा केंद्र जोधपुर भी था तो मुझे कहीं जाना नहीं पड़ा। सलेक्शन हो गया तो मैं जेएनयू चला आया। वहाँ वैश्विक स्तर के मानकों के अनुसार शिक्षा ग्रहण कर पाया। वहीं हिंदी विभाग में टाइलर विलियम्स से मुलाकात हुई, जिनके साथ मिलकर हमने विदेशी छात्रों के लिए हिंदी भाषा का एक पाठ्यक्रम बनाया और लगभग एक साल तक पढ़ाया। वहाँ से फिर ‘अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ़ इंडियन स्टडीज़’ में हिंदी पढ़ाने का मौक़ा मिला। उसी कार्यक्रम में कोलंबिया के छात्रों से मिला जिनसे कोलंबिया में हिंदी शिक्षक की वैकेंसी का पता चला। वहाँ अप्लाई किया और सलेक्शन हो गया। कोलंबिया में हिंदी और उर्दू को ‘दूसरी भाषा’ के रूप में पढ़ाने का मौक़ा मिला जो बिल्कुल ही अलग अनुभव था।
जे
आम तौर पर मैंने देखा है कि अमेरिका में जो लोग भी हिंदी पढ़ाने आते हैं, वे हिंदी भाषा के शिक्षक होकर रह जाते हैं। वे दक्षिण एशियाई विषयों को पढ़ाने का जोखिम नहीं लेते या फिर उन्हें यह मौक़ा नहीं मिलता। आपने एक तरह से यह परपंरा तोड़ी है।
दलपत
टेक्सास विश्वविद्यालय में जब मैं असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के रूप में नियुक्त हुआ तो उस समय न्यूयॉर्क में सुषम बेदी ने एक दावत रखी थी मेरे लिए। वहाँ उन्होंने भी यही बात कही कि हिंदी से साउथ एशियन स्टडीज़ शिक्षण में जाना एक नई ज़मीन तोड़ने जैसा था। अस्ल में हिंदी भाषा पढ़ाते हुए मैंने हिंदी साहित्य ख़ासकर भक्तिकाल पर शोध जारी रखा। कांफ़्रेंसेस में जाता रहा। कोलंबिया में तीन लोगों जैक हॉली, एलिशन बुश और फ्रैंसिस प्रिचेट के काम से मुझे बहुत प्रेरणा मिली। ख़ासकर जैक हॉली के भक्ति काल से जुड़े सेमिनारों से बहुत सीखा।
जे
आपकी पहली किताब ‘सुंदर के स्वप्न’ से लगता है कि यह संत कवि सुंदरदास की जीवनी है, लेकिन ऐसा है नहीं। यह एक जीवनी के ज़रिए हिंदी साहित्य के इतिहास पर और उस इतिहास को कैसे देखा जाए इस पर भी बात करती है। तो पहले आप संक्षेप में बताएँ कि यह किताब या इस शोध का ख़याल कैसे और क्यों आया?
दलपत
सुंदरदास के बारे में गहराई से मैंने एमफ़िल के दौरान सोचा, जब मैं दादूपंथ पर काम कर रहा था। दादूपंथ के संकलनों में ‘सर्वंगी’ परपंरा को पढ़ते हुए सुंदरदास के बारे में और जाना। मुझे उनका रचनाकर्म बाकी दादूपंथियों से थोड़ा अलग लगा और मैंने उनका सारा साहित्य पढ़ा ताकि उन पर शोध कर सकूँ। ‘सुंदर के स्वप्न’ में मैंने सुंदरदास को आधार बनाकर आरंभिक आधुनिक काल के पूरे साहित्यिक, आर्थिक, राजनैतिक और सामाजिक परिवेश को समझने की कोशिश की है। पारंपरिक इतिहास-ग्रंथों में काल-विभाजन के हिसाब से चूँकि सुंदरदास का समय ही ऐसा है जो भक्तिकाल की समाप्ति और रीतिकाल की शुरुआत के मिलन बिंदु पर स्थित था तो ‘भक्ति-रीति’ काल का अध्ययन ज़रूरी था।
जे
आपकी किताब की भूमिका का शीर्षक है ‘सुंदर जागा स्वप्न से’ जो मुझे अद्भुत पंक्ति लगती है।
दलपत
यह पंक्ति मैंने सबसे पहले अपने पिताजी से सुनी थी जो निर्गुण संतों के पद गाते हैं। पंक्ति कुछ यूँ है :
सपने में मेलो भयो, सपने भयो बिछोह,
सुंदर जागा स्वप्न से, न कोई मोह निर्मोह।
यह उपनिषदों में आई ‘स्वप्नावस्था’ का कथन है; यानी सपने में मिलन हुआ और सपने में ही विरह, लेकिन जब आप स्वप्न से जागे तो कोई मिलना-बिछड़ना यथार्थ रूप में था ही नहीं। यह पंक्ति उदाहरण है कि सुंदरदास ने ‘शास्त्र’ को लोक से किस तरह जोड़ा है। मैं सुंदरदास के बारे में मानता हूँ कि वह उस युग के प्रतिमानों के अनुसार उच्च शिक्षा प्राप्त संत थे जो लोक के आदर्शों पर दर्शन की बात करने में सक्षम थे।
जे
मैं सुंदरदास के जीवन और कविता के बारे में और सवाल करूँगा, लेकिन पहले एक सवाल हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में है। आप अपनी किताब में लिखते हैं कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास लिखा गया है, ख़ासकर रामचंद्र शुक्ल का इतिहास; उस पर कलोनियल ज्ञानकांड का प्रभाव है। इसे थोड़ा और स्पष्ट करें।
दलपत
हिंदी साहित्य में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति को शुक्ल जी का इतिहास पढ़ना चाहिए। यह एक कालजयी इतिहास है, लेकिन इसकी आलोचना भी हुई है और होनी भी चाहिए। हिंदी साहित्य के इतिहास में जो बड़ा योगदान शुक्ल जी का है वह यह है कि उन्होंने काल-विभाजन को केवल समय के अनुसार ही नहीं देखा वरन उनमें चल रही साहित्यिक धाराओं को पहचाना। हिंदी साहित्य का काल-विभाजन पहले से होता आ रहा था। लेकिन साहित्यिक धाराओं को पहचानकर उसे हिंदी साहित्य में प्रभावशाली ढंग से प्रतिष्ठित करने का काम शुक्ल जी ने किया। इसलिए नामवर जी कहते हैं कि शुक्ल जी को पंचांग के रूप में जो इतिहास मिला उसमें उन्होंने प्राण डालकर उसे साहित्य बना दिया। मेरा कहना है कि कालक्रम का जो ढाँचा शुक्ल जी का है, उस पर प्राच्यविदों का गहरा प्रभाव है। जैसे शुक्ल जी भक्ति और रीतिकाल से पहले के काल को वीरगाथा काल कहते हैं। असल में इस ‘वीरगाथा’ की बात जार्ज ग्रियर्सन कर चुके थे, जिसे अपने ‘इतिहास’ में वह बार्डिक पीरियड (चारण-भाट काल) का नाम देते हैं। ग्रियर्सन ने यह धारणा कर्नल जेम्स टॉड के राजपूताने के इतिहास से ली थी। टॉड राजपूताना की वीर गाथाओं को ‘फ़ेस वैल्यू’ पर लेते थे, क्योंकि राजपूताना के वीरों की तुलना में वह यूरोपीय श्वेत वीरों को देखते थे। उस दौरान टॉड के जैसा ही इतिहास मराठों का भी लिखा गया। इन ‘इतिहासों’ का प्रभाव बाद में नवजागरण के बांग्ला लेखकों पर पड़ा। इसमें बंकिमचंद्र भी का नाम लिया जा सकता है। शुक्ल जी टॉड की ही अवधारणा को आगे बढ़ाते हुए अपने ‘इतिहास’ में इसे भक्ति के उद्भव से जोड़ते हैं और भक्ति को इस्लाम के आगमन की प्रतिक्रिया दिखाते हैं। वैसे शुक्ल से पहले यही बात महावीर प्रसाद द्विवेदी भी कह चुके थे कि मुग़लकाल में अपने पौरुष से हताश हिंदू जाति भक्ति की तरफ़ मुड़ गई थी। इस अवधारणा की कमियाँ जल्दी ही सामने आईं जिसे हम हजारीप्रसाद द्विवेदी के लेखन में देख सकते हैं।
जे
पिछले दिनों हिंदी के आलोचक राजकुमार जी एक इंटरव्यू में कह रहे थे कि रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का जो इतिहास लिखा उसकी कोई भी आलोचना आज तक ठीक से नहीं की गई है। अगर यह सच है तो ऐसा क्यों है, क्योंकि अमेरिका में तो बड़े से बड़े अकादमिक लेखक के काम की आलोचना होती है।
दलपत
मैं इस बात से पूरी तरह सहमत नहीं हूँ कि शुक्ल जी के ‘इतिहास’ की आलोचना नहीं हुई है। शुक्ल जी के इतिहास के जिस हिस्से की आलोचना होनी चाहिए वह हुई है, लेकिन उन आलोचनाओं पर बात कम हुई है। जैसा कि मैंने कहा कि इस्लाम के आगमन से भक्ति को जोड़ने की शुक्ल जी की जो थीसिस थी उसे हजारीप्रसाद द्विवेदी ने ख़ारिज किया इसके अलावा शुक्ल जी के लेखन में कबीर को उचित स्थान नहीं मिला जबकि हजारी जी ने कबीर पर पूरी किताब ही लिखी है तो ये आलोचनाएँ ही हैं। जहाँ तक उनके हिंदी साहित्य के काल-विभाजन की बात है तो और भी गंभीर इतिहास लिखे गए हैं, लेकिन उनकी चर्चा न के बराबर होती है। ठीक ऐसा ही इतिहासग्रंथ गणपतिचंद्र गुप्त का ‘हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास’ है, जिसमें उन्होंने 1857 ई. के पहले के काल को ‘पूर्व आधुनिक काल’ कहा है। ‘पूर्व आधुनिक काल’ में गुप्त जी ने केवल भक्ति, रीति और वीरगाथा ही न देखकर कुल ग्यारह धाराओं की बात की है। यह इतिहासग्रंथ हिंदी साहित्य के अध्ययन में ओझल ही रहा है। भक्ति और रीतिकाल के गंभीर अध्ययन तथा आलोचना की लंबी परंपरा है, जिसमें मुक्तिबोध और विजय देव नारायण साही से लेकर रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, मैनेजर पांडेय और अभी के समय में पुरुषोत्तम अग्रवाल का काम बहुत महत्त्वपूर्ण है।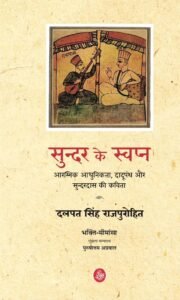
जे
अब सुंदरदास के कालखंड पर चलते हैं। आप कहते हैं कि हिंदी साहित्य में भक्ति और रीतिकाल का जो विभाजन किया गया है, वह उचित नहीं है और इसके लिए आप सुंदरदास का उदाहरण देते हैं कि वह कालक्रम के हिसाब से रीतिकाल के हैं, लेकिन उनका काम भक्तिकालीन कवियों मसलन कबीर, दादू की परंपरा में आता है। आपका यह भी कहना है कि हिंदी के आलोचकों ने रीतिकाल को मोटे तौर पर सामंती प्रवृत्ति का और ‘जबदी हुई मनोवृत्ति’ का समय कहा है, क्योंकि उस समय के कवि दरबारों का आश्रय लेते थे। आप इस पूरी समझ की आलोचना करते हैं।
दलपत
जहाँ तक रीतिकाल को समझने का काम है, उसकी आलोचना हुई है जिसमें एलिशन बुश का काम बहुत बढ़िया है। उसमें मैंने कुछ जोड़ा है। उन्नीसवीं सदी यानी कलोनियल पीरियड में साहित्य को समझने के जो मानदंड बने, अगर हम उन मानदंडों के हिसाब से भक्ति और रीतिकाल के साहित्य को समझेंगे तो दिक्कत होगी। उस मानदंड पर भक्ति काल का साहित्य तो ‘लोकजागरण’, ‘आधुनिकतापूर्ण’ और स्वतःस्फूर्त काव्य लगेगा; लेकिन रीतिकाल को समझने में समस्या होगी। रीतिकाल के मुग़ल-राजपूत दरबारी वर्ग को शासन करने में असमर्थ कलोनियल काल में ठहराया गया, जब बाद में उन्नीसवीं सदी में राष्ट्रनिर्माण और ‘साहित्य की उपयोगिता’ ‘प्रोटेस्टेंट एथिक’ तथा विक्टोरियन नैतिकता की अवधारणाएँ मज़बूत हुईं तब शृंगार रसप्रधान रीतिकविता को अश्लीलता से जोड़ा गया और नैतिक रूप से गिरा हुआ माना जाने लगा। यह समझ रीतिकाल के साहित्य को परखने में सबसे बड़ी बाधा बनी। मैंने दादूपंथ के आश्रय और विकास और सुंदरदास के साहित्य के द्वारा इस समझ की आलोचना प्रस्तुत करने की कोशिश की है।
जे
हिंदी में भक्तिकाल को रोमांटिसाइज़ किया जाता ऐसा कहकर कि यह जनता के साथ जुड़ा था। यह रूढियों का विरोध करता था और एक तरह से विरोध का प्रतीक था, लेकिन रीतिकाल के बारे में ऐसा नहीं कहा जाता है। ऐसे में इन सिद्धांतों को थोड़ा विस्तार देते हुए बताएँ कि आपका काम कैसे इस पूरी बहस को आगे बढ़ा रहा है।
दलपत
संक्षेप में कहूँ तो भक्ति की जो परंपरा है वह जिस परिवेश में उपजी है, उसे उस परिवेश में रखकर देखना चाहिए। भक्तिकाल कहते ही कि हम भक्ति के ग्रैंड नैरेटिव में फँस जाते हैं, जिसमें निर्गुण-सगुण परंपरा पर बात होने लगती है, लोक और शास्त्र की बात होती है। वैसे देखा जाए तो भक्ति को देखने के चार मॉडल विकसित हुए हैं। एक तो ‘पर्सनल डिवोशन’ का मॉडल जिसमें आराध्य को सगुण और निर्गुण के रूप में व्याख्यायित करके भक्त के संबंध को देखा गया। दूसरा मॉडल भक्ति को सामाजिक विद्रोह (सुधारवादी विचार के साथ जो भक्ति के आलोक में हो) के रूप में देखा जाए उसका रहा है; इसमें मीराबाई, कबीर, रैदास आदि की चर्चा ज़्यादा होती है। तीसरा मॉडल ‘लोक’ का है। यानी भक्ति किस तरह अपना लोकवृत्त (पब्लिक स्फ़ीयर) निर्मित कर रही थी जो कि मुग़ल-राजपूत काल में व्यापार के बढ़ने के साथ विकसित हुआ। इस मॉडल पर पुरूषोत्तम अग्रवाल का मौलिक काम है। क्रिस्चन नोवेत्सकी ने भी ‘लोक’ की अवधारणा पर शानदार काम किया है। वह कहते हैं कि संत अपने पदों के माध्यम से अपने दिक्-काल का अतिक्रमण करके ‘लोक’ में परिवर्तित होते हैं और यह लोक उन पदों को गाने वालों, उन पर चर्चा करने वालों के बढ़ाव के साथ ही विकसित होता जाता है। तो उनके अनुसार संत अपनी कविता के माध्यम से ‘लोक’ की रचना करते हैं। चौथा मॉडल ‘नेटवर्क’ का है जिस पर जैक हॉली ने लिखा है। वह कहते हैं कि भक्ति कोई एक आंदोलन नहीं है, बल्कि बहुत सारे आंदोलनों का समूह है; यानी भक्ति को उसकी बहुल आवाज़ों में देखना चाहिए। उन्होंने भक्ति को दक्षिण से आया मानने की भी आलोचना की है। भक्ति के विकास में उन्होंने मुग़ल-राजपूत शासक वर्ग की भूमिका का भी विस्तृत अध्ययन किया है। भक्ति के जो केंद्र विकसित हो रहे थे, उनके विकास में मुग़लों की भी भूमिका रही है। हॉली कहते हैं कि भक्ति अपने आश्रयदाता वर्ग के साथ संगीत, पद, चरितलेखन, संवेदना, कथा-रचना, आदि के माध्यम से अपना नेटवर्क विकसित कर रही थी। भक्ति अपने आपमें एक कलेक्टिव अवधारणा है। मैंने दादूपंथ के विकास और सुंदरदास की कविता के द्वारा भक्ति को अपने क्षेत्रीय परिवेश में स्थित करके अध्ययन करने का प्रस्ताव रखा है।
जे
इस मोड़ पर यह जानना ज़रूरी होगा कि सुंदरदास क्यों महत्त्वपूर्ण हैं। वह दादूपंथी हैं और दादू अपनी परंपरा कबीर से देखते हैं। लेकिन कबीर या दादू से इतर सुंदरदास सिर्फ़ जन से ही नहीं जुड़े हुए हैं, बल्कि उन्होंने बाक़ायदा शास्त्रों की शिक्षा ली है और उनका रचनाक्रम आर्काइव्ड है। उनके जीते जी उनका काम लिपिबद्ध हुआ है।
दलपत
सुंदरदास की जातिगत पृष्ठभूमि बनिया जाति की थी और वह बनारस में शिक्षित हुए संत थे। शिक्षा और योगाभ्यास के लिए उन्होंने वणिक जाति का अनुदान लिया था और फ़तेहपुर-शेखावटी में अपना मठ निर्मित करवाया था। उनके गुरू दादू जबकि धुनिया थे जो इस्लाम की तरफ़ झुका हुआ समुदाय था। दादू के शिष्य अलग-अलग धर्मों, जातियों से आते हैं। सुंदरदास के लिए यह स्पष्ट था कि वह ख़ुद को संत कहलवाना चाहते थे। वह संतों का और संतों के लिए साहित्य रच रहे थे। साथ ही वह संत होने की नई परिभाषा भी गढ़ रहे थे। सुंदरदास भले ही कबीर, सूर या मीराबाई की तरह आज चर्चित न हों, लेकिन आरंभिक आधुनिक काल में उनकी कविता दरबारों, लोक में और मठों आदि अलग-अलग जगहों पर तथा अलग-अलग पहचान वाले समूहों द्वारा पढ़ी जा रही थी। मैंने उनके शास्त्रीय ग्रंथ ‘ज्ञान समुद्र’ की लगभग 81 पांडुलिपियों की चर्चा अपनी पुस्तक में की है। इसका अर्थ है कि पांडुलिपि पर आधारित पठन या संस्कृति में सुंदरदास बहुचर्चित कवि थे। उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध में जब हिंदी प्रदेश में छापाख़ाना विकसित होता है तो उन छापेख़ानों में सुंदरदास जी के ग्रंथ भी बहुधा छपते हैं, लेकिन तब उनके शास्त्रीय पक्ष वाले ग्रंथों की बजाय संत-संवेदना वाले ग्रंथ जैसे ‘सवैया’ या ‘सुंदर विलास’ को ही अधिक छापा जाता है। इस प्रकार छापेख़ानों में शास्त्रीय आचार्य या दार्शनिक वाली पहचान की बजाय सुंदरदास की एक संत की छवि स्थापित होना शुरू होती है। सुंदरदास ने भक्ति को योग और अद्वैत वेदांत के साथ जोड़ने का ऐतिहासिक काम किया। भक्ति की जगह काव्यशास्त्र में भी खोजी। शास्त्रीय ज्ञान को लोकोक्ति या मुहावरों के जरिए प्रामाणिक करवाया अर्थात् लोकसंग्रह को प्रतिष्ठा दी। शास्त्रों के ज्ञान को संतभक्ति के आलोक में रचकर लोक में स्थापित करने का काम किया। वह शास्त्र और लोक के बीच में लिखित ग्रंथों के माध्यम से एक ‘ब्रिज’ का का काम कर रहे थे जो उनसे पहले के संतों में नहीं दिखता।
जे
जैसा कि आपने अपनी पुस्तक ‘सुंदर के स्वप्न’ में बताया कि सुंदरदास न केवल जनकवि थे, बल्कि उनका मिजाज़ सूफ़ियाना भी था और साथ में वेदांत जैसे विषयों पर भी गंभीर लेखन कर रहे थे। इन बातों के आलोक में आप उनकी बहुभाषा परंपरा के बारे में बताएँ। आपने अपनी किताब में त्रिभाषा और षटभाषा परंपराओं का भी ज़िक्र किया है।
दलपत
सुंदरदास ने तेरह ‘अष्टक’ लिखे हैं जो उनकी बहुभाषा यानी मल्टीलिंगुअल प्रतिभा को दर्शाता है। वह संस्कृतनिष्ठ भी लिखते हैं तो ख़ालिस फ़ारसी में भी ब्रजभाषा ‘टेम्पलेट’ में लिखते हैं। सिंधी, राजस्थानी और पंजाबी की छौंक भी उनकी कविता में है। संस्कृत के आचार्य रुद्रट जब पहले पहल ‘त्रिभाषा’ की बात करते हैं तो तीन भाषाओं में कविता लिखने की चर्चा करते हैं। बाद में भोज के संस्कृत ग्रंथों और हेमचंद्र के अपभ्रंश ग्रंथों में षटभाषा का रूपक विकसित होता है, जहाँ से यह देशभाषा में आता है। ‘पृथ्वीराज रासो’ में इसे देखा जा सकता है। षटभाषा के रूपक को अठारहवीं सदी के मध्य में भिखारीदास व्याख्यायित करते हैं। भिखारीदास कह रहे थे कि ब्रजभाषा व्यापक भाषा है जिसमें अन्य भाषाओं जैसे संस्कृत, फ़ारसी, मागधी, प्राकृत, लोकभाषाओं के शब्दों का मिश्रण हो तो वह ‘रुचिर’ बन जाती है। भिखारीदास के इस मॉडल की तुलना फ़ारसी के उनके समकालीन सिराजुद्दीन खान-ए-आरज़ू से करें तो जिस सख़्त रूप में वह फ़ारसी को डिफ़ाइन कर रहे थे, उससे ब्रजभाषा का खुलापन सामने आएगा। आरज़ू जिस तरह फ़ारसी को बाकी भारतीयों भाषाओं से काटकर उसे शुद्ध करने की कोशिश कर रहे थे, उसी तरह उन्नीसवीं सदी के पूर्वार्द्ध में राजस्थानी के सैद्धांतिक काव्यग्रंथ लिखे गए जिनमें अन्य भाषाओं से शब्द लेने को एक ‘दोष’ माना गया। ब्रजभाषा में ऐसा नहीं था इसीलिए ब्रजभाषा एक कॉस्मोपॉलिटन भाषा हो गई।
जे
अब मैं एक थोड़ा विवादास्पद सवाल पूछना चाहता हूँ। हिंदी के पब्लिक स्फ़ीयर में आम तौर पर हिंदी के इतिहास को लेकर एक तरह का कट्टरपन दिखता है। हिंदी भाषा बहुत पुरानी भाषा नहीं है और ज़ाहिर है कि जब किसी भाषा को राष्ट्र-निर्माण के काम में जोड़ दिया जाता है तो उसके कारण दूसरी भाषाएँ हाशिए पर जाती हैं। यह काम अँग्रेज़ी, तुर्की और अन्य भाषाओं में भी हुआ है। लेकिन हिंदी के कई विद्वान इसे स्वीकार नहीं करते हैं और कहते हैं कि यही प्राकृतिक था जबकि हम जानते हैं कि हिंदी के कारण ब्रज, अवधी, बुंदेलखंडी, राजस्थानी, मैथिली, मगही जैसी की भाषाओं का नुक़सान हुआ है।
दलपत
छायावाद के स्तंभ कवि सुमित्रानंदन पंत ‘पल्लव’ पत्रिका की भूमिका में लिखते हैं कि हमें भाषा की नहीं बल्कि राष्ट्रभाषा की ज़रूरत है। ब्रजभाषा में रात्रि का आलस्य है तो खड़ी बोली में सुबह के जागरण का उद्-घोष। कृष्ण को मुरली की नहीं पाञ्चजन्य की आवश्यकता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी भी कहते हैं कि यमुना किनारे केलि करने का समय ख़त्म हुआ और अब कवियों को राष्ट्र-निर्माण में प्रवृत्त हो जाना चाहिए। असल में राष्ट्र-निर्माण के प्रतिमान जब आते हैं तो ब्रजभाषा के जैसी अन्य भाषाएँ हिंदी की ‘बोलियाँ’ बन जाती हैं। फिर हिंदी के अध्ययन-अध्यापन में राजस्थानी, मैथिली को तो छोड़ ही दीजिए, ब्रजभाषा और अवधी का अध्ययन भी ठीक से नहीं हो पाता। इन भाषाओं में आज जो साहित्य रचा जा रहा है उसे ‘हिंदी’ में स्थान नहीं मिलता। हिंदी ने अपने ‘प्रतिमान’ स्वरूप राष्ट्रीय जागरण में जो भूमिका निभाई उससे आगे जाने की ज़रूरत है, क्योंकि वह अब इतिहास की वस्तु है। ब्रजभाषा की साहित्यिक संस्कृति एक आदर्श है कि आज की हिंदी को अपनी ‘बोलियों’—जो स्वतंत्र भाषाएँ हैं—से किस तरह का संबंध रखना चाहिए।
जे
और अंत में आपकी नई किताब के बारे में बताएँ।
दलपत
मेरी नई किताब ‘इन द श्राइन ऑफ़ द हार्ट’ जर्मनी की विद्वान मोनिका हार्स्टमैन के साथ है। हमने एक वृहत्तर अँग्रेज़ी पाठक-समुदाय को ध्यान में रखकर सोलहवीं-सत्रहवीं सदी के सात संतों का अध्ययन किया है। ये संत हरदास, दादू, संतदास, रज्जब, सुंदरदास, बखना और बाजीद हैं जो सभी राजस्थान के संत हैं। हमने राजस्थान के ऐतिहासिक परिवेश, साहित्यिक संस्कृति, भक्ति आंदोलन, और सामुदायिक संदर्भ में इन संतों की कविता और दर्शन को देखा है। किताब के तीन बड़े अध्याय हैं। पहले में राजस्थान में भक्ति के उद्भव, संतों के दर्शन, पद गायन-पठन की परंपरा, पांडुलिपियाँ, और संत काव्य रूपों का विस्तृत अध्ययन किया है। दूसरे अध्याय में संतों के आश्रय और ‘नेटवर्क’ का अध्ययन किया है जिसमें फ़तहपुर, सांगानेर, डीडवाना, आमेर, साम्भर, नरैना आदि क़स्बों के इतिहास को भी वहाँ हो रहे दादूपंथ के विकास के क्रम में देखा गया है। तीसरे अध्याय में सातों कवियों की कविताओं का अँग्रेज़ी में अनुवाद है। हमने इन संतों के कुछ अप्रकाशित ग्रंथों को भी पहली बार इस किताब में प्रकाशित किया है। संत-कविता के परफ़ॉरमेंस के ऑडियो-वीडियो के लिंक भी पुस्तक में जगह-जगह दिए हैं और संत कविता की जीवंतता को दर्शाने की कोशिश की है।
जे सुशील से परिचय के लिए यहाँ देखें : ‘किसी किशोरवय बालक की तरह लोग हिंदी में प्रयोग करते हैं’

