नस्र ::
तसनीफ़ हैदर
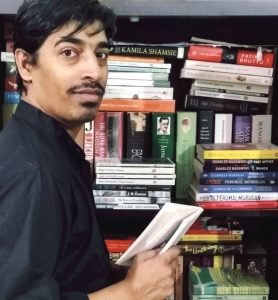
कलकत्ता शहर मैंने कभी नहीं देखा। मालूम है कि वहाँ ग़ालिब ने अठन्नी पर शानदार हवेली किराए पर ली थी, ये भी जानता हूँ कि दाग़ की महबूबा यहीं रहा करती थीं। फोर्ट विलियम कॉलेज, उर्दू के क्लासिकल टेक्स्ट की तैयारी का वो दौर और हिंदुस्तान की राजधानी होने का गर्व। यानी कलकत्ता के दामन में क्या कुछ नहीं रह चुका है। ईडन गार्डन, मोहन बगान और हावड़ा ब्रिज के नाम हम बहुत पहले से सुनते चले आए हैं। कभी बड़ों की ज़बानी, कभी दोस्तों की तो कभी किताबों की। मगर अब की बार रवींद्रनाथ टैगोर ने उन्नीसवीं सदी के अंतकाल में मौजूद कलकत्ता शहर के दर्शन करवाए, और ऐसे करवाए कि वहाँ के घरों में ले गए, वहाँ के लोगों से मिलवाया, बंगालियों का मिज़ाज समझाया, उनके रीति रिवाज, उनकी रस्में, हिंदू मुसलमानों का अँग्रेज़ हुकूमत के ख़िलाफ़ एकजुट होकर लड़ना और हिंदू धर्म, ब्राह्मणवाद और ब्रह्म-समाज की कश्मकश को भी आँखों पर नुमायाँ करवाया।
उस दौर में मौजूद लड़कियों और औरतों के घरेलू और शिक्षा के मुआमलों को उजागर किया। मर्दों की भिन्न प्रकार की सोचें, आम ज़िंदगियों में अख़बार की अहमियत और मज़हब के साथ-साथ समाज की सख़्ती और पाबंदी पर भी ऐसी-ऐसी बहस करवाई कि हम वाक़िफ़ हो सके कि उस दौर में जहाँ से टैगोर अपने शहर, अपनी रियासत और अपने देश को देख रहे थे, उसमें उन्हें किस क़िस्म की मुश्किलात दिखाई दे रही थीं, वो कैसे मसले थे, जिनमें से बहुत से अभी भी हमारी गर्दनों में ज़ंजीरों की तरह पड़े हुए हैं और इस ज़माने में ‘गोरा’ को पढ़ कर हमें क्या फ़ायदा हासिल होगा?
मुझे महसूस होता है कि ‘गोरा’ एक ऐसा नॉविल है, जिसका वाचन हमें ये समझाने के लिए काफ़ी है कि इंसान जब तक धार्मिक उपदेशों और कट्टर रीति-रिवाज के चक्कर में पड़कर अपना वक़्त बर्बाद करता रहेगा, तब तक उसके लिए एक ऐसे समाज की कल्पना असंभव है, जहाँ सबके लिए बराबरी के मौक़े मयस्सर आ सकें। टैगोर इस बराबरी के फ़लसफ़े पर प्रगतिशील लेखकों जैसा आग्रह नहीं करते हैं, बल्कि उनका मानना है कि इंसान किसी भी धर्म से तअल्लुक़ रखता हो, उसे बस अपनी सच्चाई को समझना चाहिए, उसे सोचना चाहिए कि ख़ुदा इतना मामूली और ऐसा हल्का नहीं हो सकता कि इंसानों में ऊँच-नीच और बँटवारे जैसी चीज़ों को परवान चढ़ाए। किसी को ब्राह्मण बनाकर उसे ऊँची गद्दियों पर बिठा दे और किसी को शूद्र बनाकर उसे पस्तियों में फेंक दे।
टैगोर के नॉविल से मालूम होता है कि उन्नीसवीं और बीसवीं शताब्दी के दरमियान झूलता हुआ बंगाल, कैसे दो मुख़्तलिफ़ सोचों के लिए महाभारत का मैदान बना हुआ था। एक तरफ़ ब्रह्म-समाज के लोग थे, जो तालीम और नई तहज़ीब को अपनाकर अँग्रेज़ों की ख़ुशनूदी हासिल करना चाहते थे तो दूसरी तरफ़ कट्टरवादी हिंदू, जिनकी सोच उन्हें लगातार बीते हुए कल की तरफ़ धकेलती हुई महसूस होती थी। दोनों ही वर्ग अपनी अपनी कोशिशों और मुआमलों में इंतिहा पर पहुँचे हुए थे, दोनों एक दूसरे के सख़्त विरोधी थे और कई बार तो ये विरोध, नफ़रत और किनारा-कशी की सूरत भी इख़्तियार कर लेता था।
टैगोर ने दोनों ही वर्गों की कहानी में ही सकारात्मक आलोचना की है। दोनों ही जानिब कट्टर क़िस्म के लोग भी थे, जैसे ब्रह्म-समाज में हरण बाबू (जो अपने अहंकार के कारण हिंदू धर्म के लोगों को नीच, अनपढ़ और दक़यानूसी कहकर रद्द करते थे) तो दूसरी तरफ़ हिंदू धर्म के मानने वाले गोरा और अविनाश जैसे लोग (जो अपनी रूढ़िवादी सोच के आगे इतने मजबूर थे कि) भारत पर अँग्रेज़ों के क़ब्ज़े को अपने बुज़ुर्गों का एक महापाप समझकर हवन के ज़रिए उसका प्रायश्चित करना चाहते थे।
टैगोर ने ब्रह्म-समाज पर ये सवाल उठाया है कि वो अपनी बुनियादों को अलग करके, हिंदुस्तान के एक बड़े हिस्से को काटकर कैसे उसकी भलाई का दावा कर सकता है; जबकि कट्टरपंथियों पर उनका ये आरोप है कि धार्मिक उपदेशों के नाम पर इंसान को बाँटना, उसे सामाजिक ज़ुल्म की भेंट चढ़ा देना है, छुआछूत और बात-बात पर इंसान को इंसानियत से गिरी हुई कोई चीज़ समझने से क्या हिंदू धर्म के ख़िलाफ़ इसी के मानने वालों में एक तरह की असुरक्षा का भाव नहीं पैदा होगा?
टैगोर ने इस दास्तान में साफ़-साफ़ समझाने की कोशिश की है कि इंसान को दूसरों पर अपना मज़हब या नज़रिया लादने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। एक ऐसा समाज जहाँ बहुत से धर्मों के मानने वाले, बहुत से वर्गों में बँटे हुए लोग हों, वहाँ समझौते के रास्ते निकालकर सबको एकजुट रखने की कोशिश करनी चाहिए। तालीम का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। बर्दाश्त और मोहब्बत के जज़्बों को जिस क़दर आम हो सके, उतना आम करना चाहिए। टैगोर इस बात से असहमत हैं कि किसी पर क्रिश्चियन होने का इल्ज़ाम लगाया जाए या किसी को ज़ात बिरादरी बाहर करने का मशविरा दिया जाए। इस तरह की बातों से उनके नज़दीक लोगों को सिर्फ बाँटा जा सकता है।
टैगोर ने नॉविल में इसी लिए ऐसे मज़बूत किरदार के लोग भी दोनों जानिब रखे हैं, जिनसे नेकी और मोहब्बत के बर्ताव की बेहतर मिसाल क़ायम करने में मदद मिल सके। इसलिए ब्रह्म-समाज में एक तरफ़ परेश बाबू हैं तो वहीं सख़्त-गीर हिंदू घराने में जन्म लेने वाली आनंदमई भी हैं। परेश बाबू और आनंदमई दोनों दो बूढ़े, तजुर्बेकार और ज़माने के सर्द-ओ-गर्म झेले हुए लोग हैं, जो समाज का विरोध और उसके तानों, तिश्नों का खुलकर मुक़ाबला करते हैं। जो प्रेम में निस्वार्थ हैं और जिनके पास अपने कर्मों के लिए दूसरों से कई गुना बेहतर कारण मौजूद हैं। टैगोर ने इन्हीं के ज़रिए नॉविल में नकारात्मक सामाजिक लहर को चुटकियों में उड़ाने का काम किया है।
उनका मानना है कि इंसान अगर सच्चाई को समझता हो, जानता हो और उसके दिल में इंसानों से मोहब्बत का जज़्बा हो तो वो किसी भी तरह की मुश्किल को झेलने में नाकाम नहीं होगा। इंसान मुश्किलों से तब तक ही डरता है, जब तक उसके दिल में अपने फ़ैसलों के तअल्लुक़ से कोई कश्मकश मौजूद हो। मुकम्मल यक़ीन और आख़री दर्जे की मोहब्बत जहाँ मौजूद हो, वहाँ इंसान पर लगा हुआ कोई भी इल्ज़ाम या उस के ख़िलाफ़ की जाने वाली कैसी भी साज़िश उसे अपने फ़ैसले से पीछे नहीं हटा सकती। इन दो बूढ़े किरदारों में भी परेश बाबू का रुझान अपने लोगों की जानिब झुकता हुआ भी महसूस होता है, वो उनके क्रोध के बावजूद उनके लिए दिल में बड़े आदर का जज़्बा भी रखते हैं और उनके सामने सफ़ाई भी पेश करते हैं।
जबकि आनंदमई जैसी बूढ़ी औरत, जिसे आख़िर में टैगोर ने भारत माता के समान माना है, किसी भी तरह का ख़ौफ़ नहीं पालतीं, न वो सफ़ाई देती हैं, न वो अपने वर्ग तक सीमित होने का कोई दावा करती हैं। उनका दिल इतना बड़ा मालूम होता है कि इसमें हर मज़हब और हर समाज से तअल्लुक़ रखने वाले शख़्स के लिए जगह हो सकती है। इसी लिए जब ब्रह्म-समाज की लड़की लोलिता और हिंदू धर्म को मानने वाला विनय शादी का इरादा करते हैं तो आनंदमई ही होती हैं, जो न सिर्फ़ इन दोनों की शादी में शरीक होती हैं, बल्कि दोनों वर्गों से जुड़े लोगों के दरमियान पुल का-सा काम करती हैं।
इस नॉविल को पढ़कर उस दौर में बंगाली औरतों की हालत का अंदाज़ा भी होता है। एक तरफ़ आनंदमई जैसी औरतें तो हैं ही, जो किसी भी तूफ़ान से टकराने की हिम्मत रखती हैं, मगर दूसरी तरफ़ हरी मोहिनी जैसी औरतों का किरदार भी बहुत कुछ जानने और समझने में मदद देता है। ऐसी औरत, जिसका पति मर जाए, उसकी हालत समाज में किस क़दर नाज़ुक हो जाती है और वो जायदाद, लालची रिश्तेदारों और सामाजिक मसलों के त्रिकोण में कैसे घिरकर रह जाती है। हरी मोहिनी का किरदार न सिर्फ़ हिंदू औरतों की बुरी हालत का बयान है, बल्कि ख़ासतौर पर इंसान की एक अजीब कमज़ोरी की तरफ़ भी लेखक ने इस किरदार के ज़रिए इशारा किया है। आदमी के हाथों से जब दुनिया निकल रही हो, खिसक रही हो, लोग उसे छोड़ रहे हों, उसके पास कोई अपना न हो, वो बहुत पतली हालत का शिकार हो तो ऐसे में वो भगवान से डरने वाला और पूजा-पाठ में वक़्त बिताने वाला इंसान बन जाया करता है।
मगर जैसे ही हालात बदलते हैं, वक़्त करवट लेता है, उसके पास रहने सहने का अच्छा ठिकाना हो जाता है, माल मयस्सर आ जाता है, राहत मिल जाती है और कोई खटका नहीं रहता तो आदमी फिर उसी अकड़ का शिकार हो जाता है, जैसा कि वो ग़रीब और लाचार होने से पहले हुआ करता था और इसका इंसान की उम्र से कोई तअल्लुक़ नहीं, बल्कि उसकी फ़ितरत से है।
गोरा नामी इस नॉविल का प्रसंग कहीं न कहीं समाज है। इस नॉविल का मुख्य किरदार ‘गुरू मोहन बाबू उर्फ़ गोरा’ जो कि सामाजिक पाबंदियों को धर्म की दृढ़ता की एक शक्ल मानता है और दूसरों को गर्मागर्म बहसों से ये बात मनवाता भी रहता है, वो भी जब ज़मीन पर चक्कर लगाता है, कलकत्ता से आगे देहातों में घूमता-फिरता है तब उस पर ये नंगी हक़ीक़त रौशन होती है कि समाज किस तरह धर्म के नाम पर अपना उल्लू सीधा करता है और जो पाबंदियाँ समय के साथ अपनी शक्ल नहीं बदलतीं वो कैसे कुछ ख़ास लोगों के लिए उम्दा आर्थिक साधनों में बदल जाती हैं और किस तरह अवाम के एक बड़े हिस्से के लिए ज़ुलम-ओ-जब्र की शक्ल इख़्तियार कर लेती हैं। क्यों ऐसे समाज में बेटियाँ पैदा करना जुर्म हो जाता है और मज़हबी बरतरी के नाम पर लोगों को बेवक़ूफ़ बनाना आसान होता जाता है, उनकी जेबों को ऐंठा जा सकता है।
होने को तो ये एक सदी पुराना नॉविल है, मगर हम जिस दौर में जी रहे हैं, उसमें ‘गोरा’ में दिखाई जाने वाली हक़ीक़तें हमसे बहुत दूर नहीं हैं। हम कोई भी मज़हब मानने वाले हों, किसी भी वर्ग से तअल्लुक़ रक्खें। हम सबके सब एक ही बात से बेवक़ूफ़ बनाए जाते हैं, एक ही बात को तीर की तरह आज़माते हैं कि फ़लाँ साहब पर तो पश्चिमी सभ्यता का बड़ा प्रभाव है। हम नई, बेहतर या सुलझी हुई फ़िक्र को जल्द से जल्द पश्चिम से जोड़कर अपना पीछा उससे छुड़ाते वक़्त भूल जाते हैं कि हम साथ ही साथ अपनी कट्टरता और दक़यानूसीपन का खुल्लमखुल्ला इज़हार कर रहे हैं। गोरा में किसी जगह परेश बाबू किसी को समाज के बारे में विस्तार से समझाते हैं, जिसका अर्थ है कि जो समाज ख़ुद को बदलने पर राज़ी नहीं, उससे लिपटे हुए धार्मिक उपदेश उसी के लिए ख़ून चूसने वाले कीड़े की सूरत में ढल जाते हैं।
माफ़ कीजिएगा, शीर्षक देखकर आपको लगा होगा कि मैं कहानी के प्लॉट के बारे में बताऊँगा, किरदारों का परिचय दूँगा। नॉविल की रचनात्मक कमज़ोरियों और ख़ूबियों को गिनवाऊँगा। ये सब मेरे काम नहीं हैं। हर वो पाठक जो इस नॉविल को पढ़ेगा, अपनी जानिब से इसकी सृजनात्मक कमज़ोरियों और ख़ूबियों का फ़ैसला करेगा। कहानी इतनी दिलचस्प है कि अगर उसे इतने से मज़मून में बयान किया जा सकता तो टैगोर क़रीब सात सौ पन्नों का ये नॉविल क्यों लिखते, एक छोटी-सी कहानी लिखकर बात न ख़त्म कर देते? एक छोटी कहानी या नॉविल के बीच बड़ा अंतर दरअसल किसी सब्जेक्ट पर नॉविल लिखने वाले के ख़यालात की मुख़्तसर या विस्तार से की गई बहस ही है, वरना कहानी क्या है, उसे तो वनलाइनर में भी बयान किया जा सकता है।
आज ‘गोरा’ जैसे नॉविल इसलिए पढ़े जाने चाहिए क्योंकि हम सब भी एक बग़ल में मज़हब और दूसरे में समाज की मुक़द्दस क़ानूनी किताबें लिए घूम रहे हैं। हमारे लिए हमारे समाज और हमारे मज़हब या फ़िरक़े पर की गई कोई भी आलोचना नाक़ाबिल-ए-बर्दाश्त है। हम अपने आसमानी सहीफ़ों पर किसी के इनकार को उनकी निंदा समझते हैं। हमारे नज़दीक पवित्रता का मतलब ही ये है कि दूसरे इंसान को या तो अपने मज़हब पर राय देने से बाज़ ही रखा जाए या फिर उसको नासमझ, जाहिल, समाज के लिए ख़तरा या फिर गुस्ताख़ वग़ैरह क़रार देकर ठिकाने लगाने की कोशिश की जाए।
हम आज भी कहीं न कहीं दूसरों को बिरादरी बाहर कर देने की बेवक़ूफ़ी को बड़ा नैतिक क़दम उठाने के बराबर समझते हैं। सवाल पूछने से डरते हैं और सवाल पूछने वालों को शक की निगाह से देखते हैं। हमें इस नॉविल का पाठ करने से इसलिए भी फ़ायदा होगा क्योंकि हम मोहब्बत करना भूल चुके हैं, मोहब्बत करते भी हैं तो ज़रा-ज़रा-सी सामाजिक या धार्मिक रुकावटों की वजह से डर जाते हैं, पीछे हट जाते हैं। लोलिता और विनय की मोहब्बत का फ़साना इस नॉविल में ख़ासतौर पर नौजवानों को ये बात समझाने के लिए काफ़ी है कि जिन दिलों में अपनी ही मोहब्बत की इज़्ज़त न हो, उसी को हासिल करने की हिम्मत न हो, उसकी सच्चाई को मानने का हौसला न हो; वो वतन, मज़हब, समाज या ख़ानदान से लगाव का कितना ही दावा करते रहें, झूठे ही रहेंगे।
…इन सब बातों की वजह से अगर जी में आए तो ये नॉविल पढ़िए और अपने दोस्तों को भी पढ़वाइए। मैंने ये नॉविल अपने दोस्त फ़ैज़ रिज़वी की मदद से जामिया की लाइब्रेरी से निकलवाकर उर्दू में पढ़ा था, जिसका तर्जुमा सज्जाद ज़हीर ने किया है, और किताब साहित्य अकादेमी से क़रीब पचपन बरस पहले शाया हुई है।
![]() तसनीफ़ हैदर उर्दू की नई नस्ल से वाबस्ता कवि-लेखक हैं। ‘सदानीरा’ पर समय-समय पर शाया उनके कामकाज को उनके ही लिप्यंतरण/अनुवाद में पढ़ने के लिए यहाँ देखें : तसनीफ़ हैदर
तसनीफ़ हैदर उर्दू की नई नस्ल से वाबस्ता कवि-लेखक हैं। ‘सदानीरा’ पर समय-समय पर शाया उनके कामकाज को उनके ही लिप्यंतरण/अनुवाद में पढ़ने के लिए यहाँ देखें : तसनीफ़ हैदर
